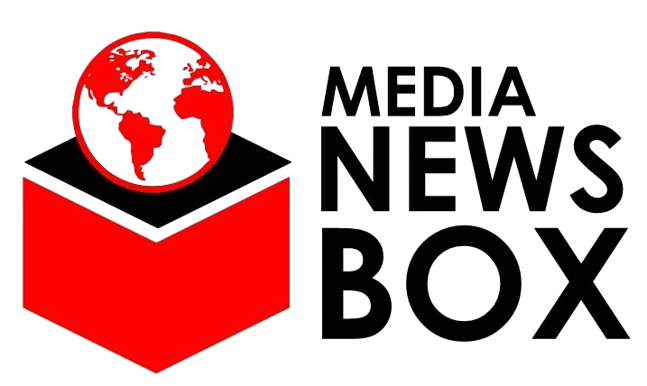भारत को मध्यम वर्ग की अपनी परिभाषा में संशोधन करना चाहिए। 1 करोड़ रुपये कमाने वाले अब ‘अमीर’ नहीं हैं।
India must revise its definition of middle class

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगला बजट, जो बस कुछ ही सप्ताह दूर है, को केवल गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की राजनीतिक रूप से आकर्षक धारणा से दूर जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार को दो चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए: मध्यम वर्ग के रूप में जो माना जाता है उसे संशोधित करना और इस समूह के लिए कर प्रोत्साहन को लक्षित करना। वर्तमान में, मध्यम वर्ग की स्वीकृत परिभाषाएँ आर्थिक विकास के वास्तविक प्रमुख प्रेरकों को बाहर करती हैं। संक्षेप में, आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्यम वर्ग की वर्तमान परिभाषाओं से अधिक कमाता है, लेकिन जीवन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वास्तविक अर्थ में अमीर नहीं है। यह वह वर्ग है, जो सालाना 1 करोड़ रुपये तक कमाता है, जिसे अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्र के मूड के लिए भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मध्यम वर्ग की परिभाषा में संशोधन करें सबसे पहले, सरकार को इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है कि वह मध्यम वर्ग को क्या मानती है। राजनीतिक अर्थशास्त्री मिलन वैष्णव ने 2017 में एक शोधपत्र में उस समय के विभिन्न अनुमानों को शामिल करते हुए एक आसान तालिका प्रदान की।
मौजूदा साहित्य में भारतीय मध्यम वर्ग को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी आय $3,650 प्रति वर्ष - जो वर्तमान विनिमय दरों पर केवल 3.1 लाख रुपये होगी - से लेकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। यह एक हास्यास्पद रूप से पुराना अनुमान है, खासकर जब ऊपरी सीमा की बात आती है।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, जो आज भी लागू है, 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का उच्चतम कर स्लैब लगता था। नई व्यवस्था ने इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया, जो शायद ही कोई सुधार है। मूल रूप से, कर विभाग के अनुसार, यदि आप इतनी राशि कमाते हैं तो आप निश्चित रूप से अमीर हैं। और इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है।
आयकर विभाग के निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार करें: 2011-12 में 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय की रिपोर्ट करने वाले लोग सभी आयकर दाखिलकर्ताओं का केवल 3.7 प्रतिशत थे। यह अनुपात 2022-23 तक बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया, जो चार गुना से भी ज़्यादा है।
कर दाखिल करने वालों का यह 16.2 प्रतिशत 2022-23 में व्यक्तियों द्वारा चुकाए गए सभी करों का एक तिहाई हिस्सा है। बेशक, इसका कुछ हिस्सा बेहतर अनुपालन से जुड़ा है, लेकिन बेहतर अनुपालन को मोटे तौर पर सभी अन्य आय समूहों पर भी लागू किया जाना चाहिए था। जो हुआ है वह यह है कि इस ब्रैकेट में कमाने वाले लोगों की संख्या - 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष - भी बढ़ी है।
याद रखें, यह सिर्फ़ आयकर दाखिल करने वालों की बात है। ब्रैकेट में कमाने वाले लेकिन कर दाखिल नहीं करने वाले लोगों की संख्या अभी भी, दुर्भाग्य से, कहीं ज़्यादा है।
मध्यम वर्ग की अवधारणा को संशोधित करने का दूसरा चरण व्यय को देखना है। मध्यम वर्ग लोगों का वह समूह है जिसके पास - ओवरहेड्स और बचत का हिसाब लगाने के बाद - विशिष्ट उपभोग के लिए पैसा बचा रहता है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है।
उपभोग पैटर्न का विश्लेषण
2023-24 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से पता चलता है कि औसत शहरी परिवार अपने कुल मासिक खर्च का लगभग 40 प्रतिशत भोजन पर खर्च करता है। अन्य छह प्रतिशत क्रमशः शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होता है। परिवहन पर लगभग 8.5 प्रतिशत, किराए पर 6.6 प्रतिशत और ईंधन पर 5.5 प्रतिशत खर्च होता है। तो, यह सामान्य ओवरहेड पर खर्च का लगभग 65 प्रतिशत है।
यह, ज़ाहिर है, औसत है। शिक्षा मुद्रास्फीति की व्यापकता - जैसा कि दिप्रिंट की फ़रीहा इफ़्तिख़ार ने यहाँ और यहाँ बड़े पैमाने पर दिखाया है - का अर्थ है कि शिक्षा की वास्तविक लागत शायद आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा के लिए भी यही सच है।
लेकिन अभी के लिए 65 प्रतिशत के आधिकारिक आँकड़ों पर चलते हैं। लगभग 30 प्रतिशत अधिक खर्च ऐसे खर्चों में जाता है जो बिल्कुल नियमित नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, जैसे कपड़े, बिस्तर, जूते और घर की मरम्मत।
सालाना 10-15 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए, ये सभी खर्च 30 प्रतिशत कर (अधिभार को छोड़कर) के अतिरिक्त हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट आ रही है।
इसके अलावा, कराधान के इस स्तर से विशिष्ट उपभोग के लिए क्या बचता है? बाहर खाना, फिल्में देखना, उपभोक्ता सामान खरीदना, यात्रा करना और सामान्य उपभोग व्यय, ये सभी अधिकांश लोगों की आय का एक छोटा सा हिस्सा है - अगर ऐसा होता भी है।
अब, आइए देखें कि अब तक कर प्रोत्साहन किस तरह से संरचित किए गए हैं। हाल के दिनों में उनमें से लगभग सभी उन लोगों के लिए लक्षित थे जिनकी सालाना आय 7-10 लाख रुपये से कम है। यह अच्छा था, और इससे उन लोगों को मदद मिलती। लेकिन इससे कुल मिलाकर आर्थिक प्रोत्साहन मामूली था। इस वर्ग में आय इतनी अधिक नहीं है कि कर कटौती उपभोग व्यय पर सार्थक प्रभाव डाल सके।
इसके बाद, कल्पना करें कि 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले सभी लोगों को केवल 20 प्रतिशत आयकर देना होगा, जो कि अभी उन्हें 30-40 प्रतिशत देना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। लोगों को अच्छा समय बिताना पसंद है और जब वे इसे वहन कर सकते हैं, तो वे ऐसा करते हैं।
राजस्व निहितार्थ
राजस्व निहितार्थ के बारे में क्या? मैंने पिछले कॉलम में तर्क दिया था कि सरकार आयकर में कटौती नहीं कर सकती क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी दोनों ही उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं।
मैंने यह गणित नहीं लगाया है कि अगर 10 लाख से 1 करोड़ रुपये की आय वाले लोगों के लिए कर की दर घटाकर 20 प्रतिशत कर दी जाए तो क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अधिक खपत और इस श्रेणी में लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण जीएसटी संग्रह में वृद्धि से इसकी भरपाई हो जाएगी क्योंकि इस तरह की खपत विकास को बढ़ावा देती है और कुल आय को बढ़ाती है।
कर अधिकारियों को निश्चित रूप से इस बात की बेहतर समझ होगी कि राजस्व निहितार्थ क्या होंगे। लेकिन उन्हें कम से कम मध्यम वर्ग की इस विस्तारित परिभाषा के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए और खुद को 10 लाख रुपये प्रति वर्ष की पुरानी सीमा से मुक्त करना चाहिए।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे अर्थव्यवस्था का मूड बदल जाएगा। एक सामान्य और व्यापक निराशा है जो बड़े पैमाने पर मुखर मध्यम वर्ग (मेरी परिभाषा) द्वारा भड़काई गई है जो इस बात की शिकायत कर रहा है कि वे कर के रूप में कितना भुगतान करते हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में उन्हें बदले में कितना कम मिलता है।
इन लोगों को आराम करने दें। सरकार के पक्ष में उनकी ऊंची आवाज को उठने दें। उन्हें खर्च करने दें। और देखें कि कैसे देश का मूड बदलता है, और विकास तेजी से वापस आता है।